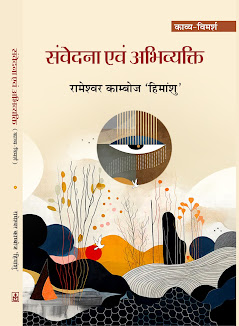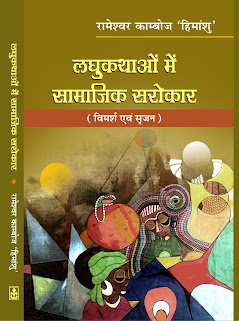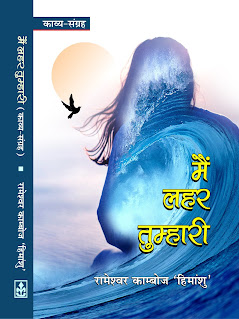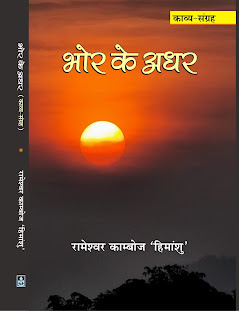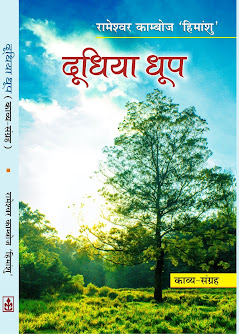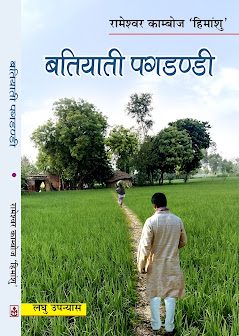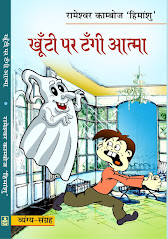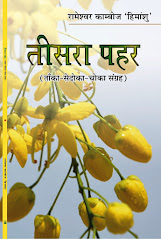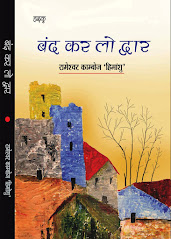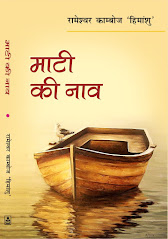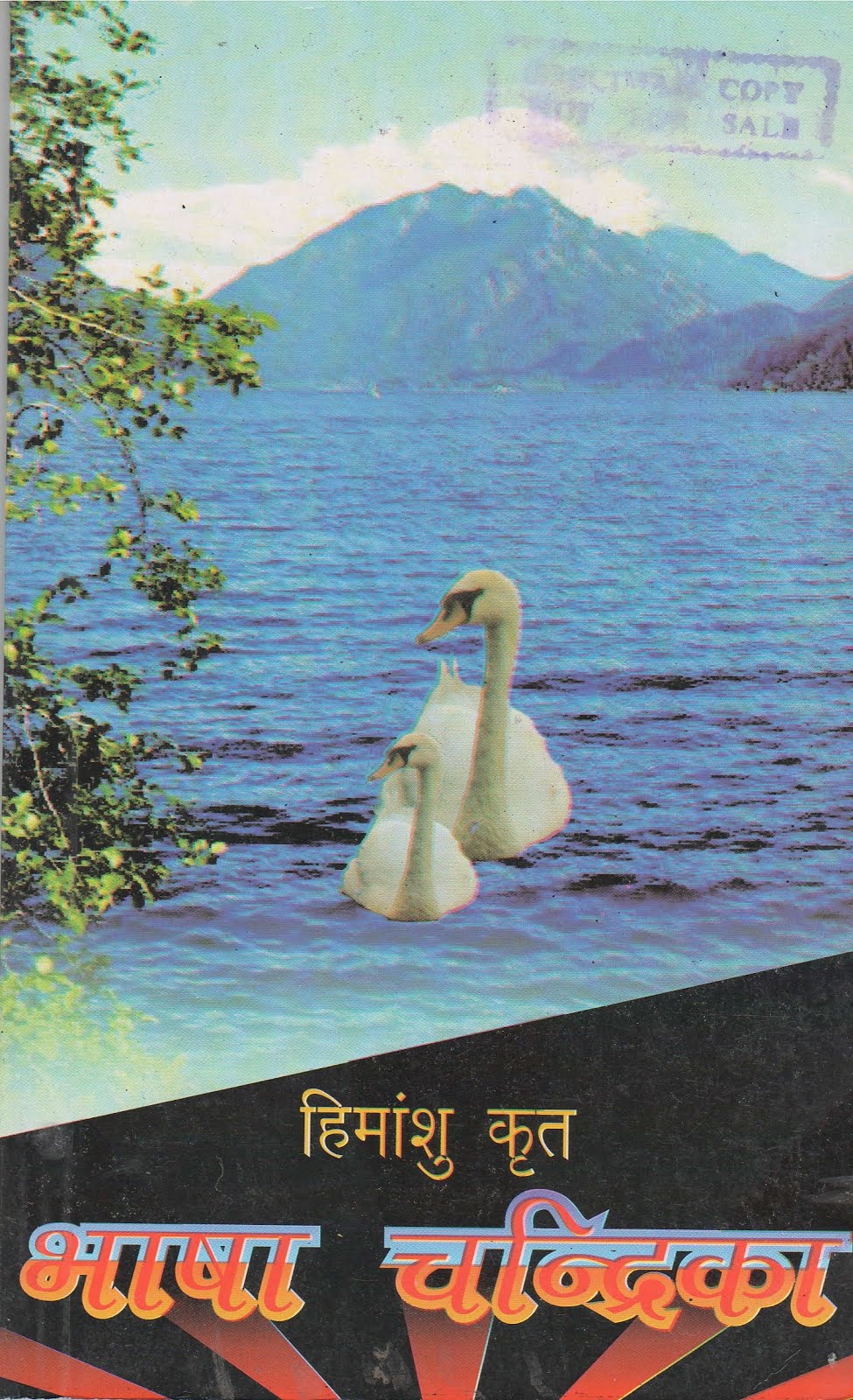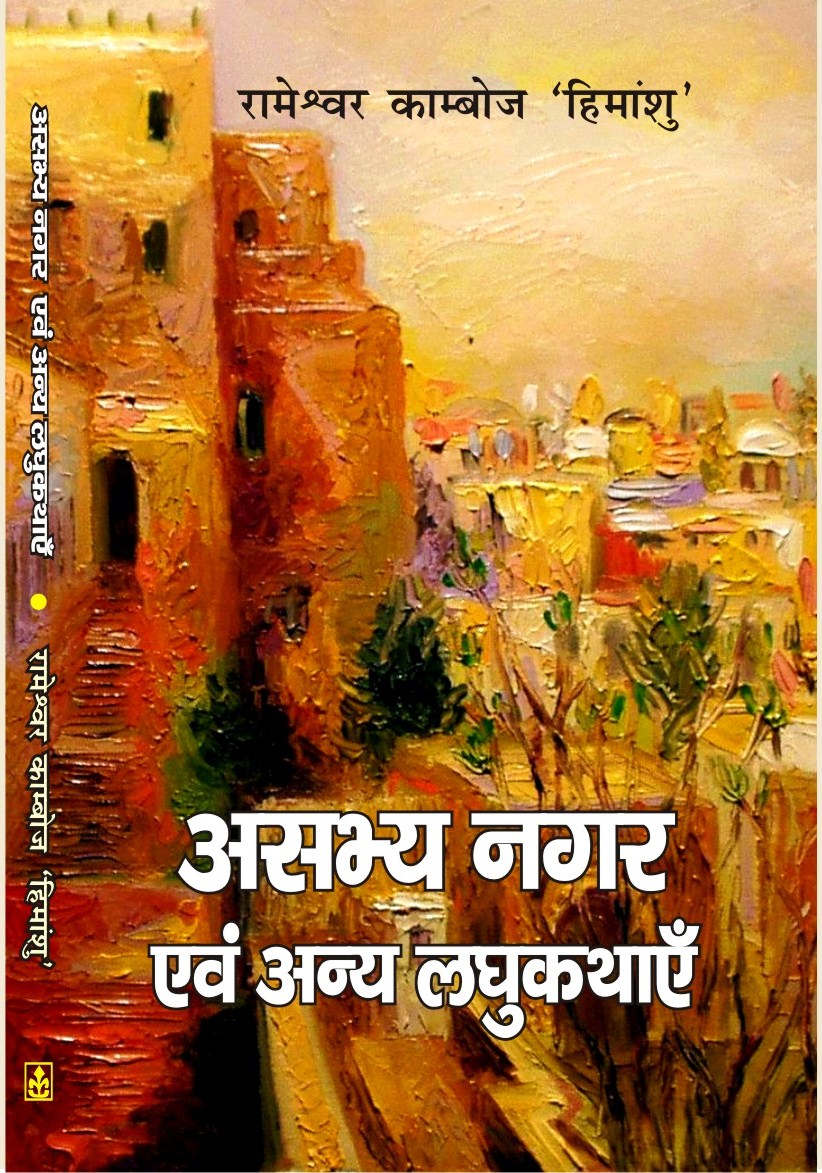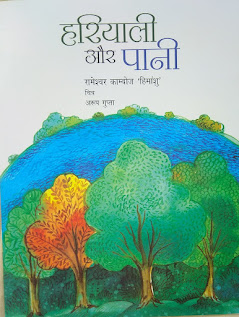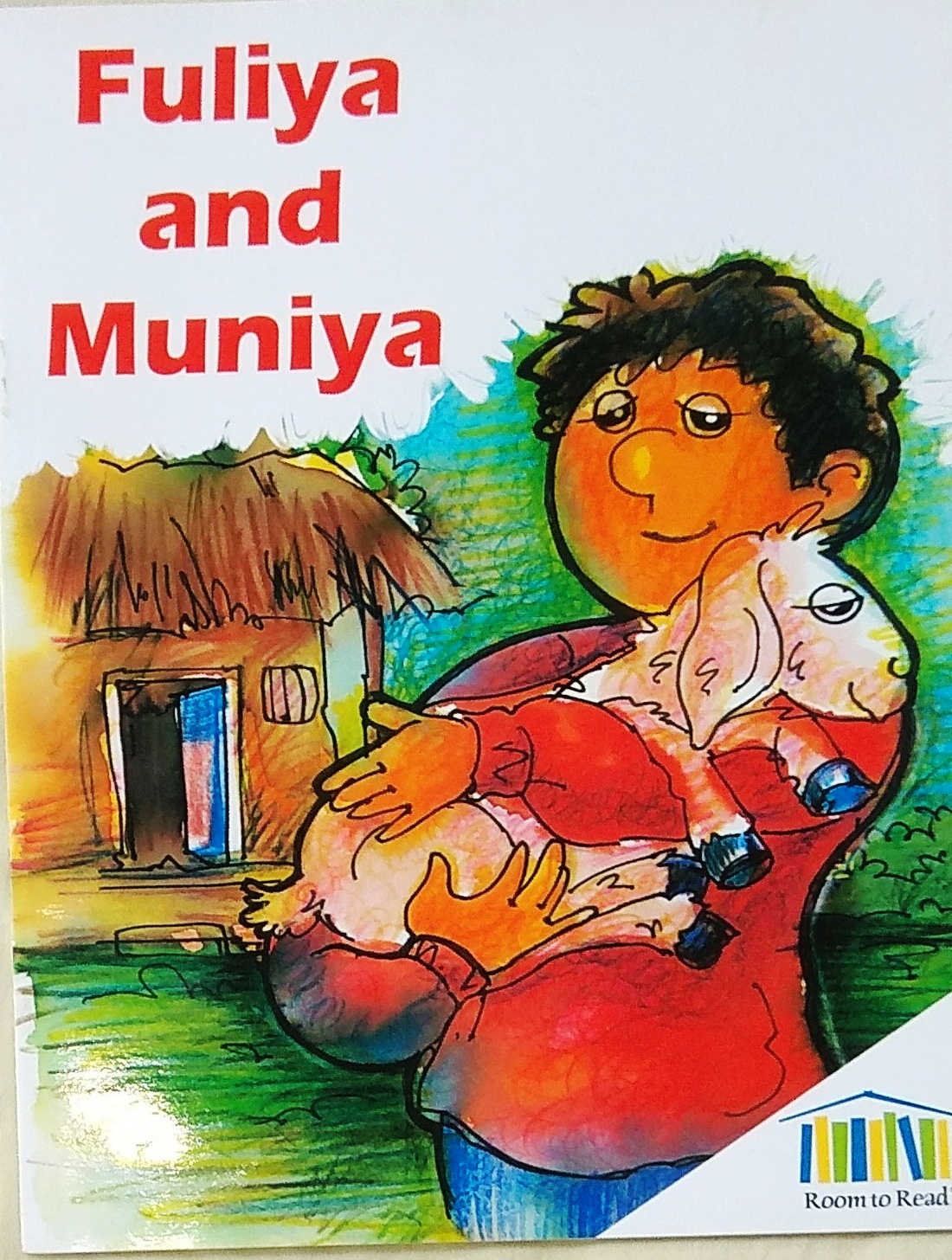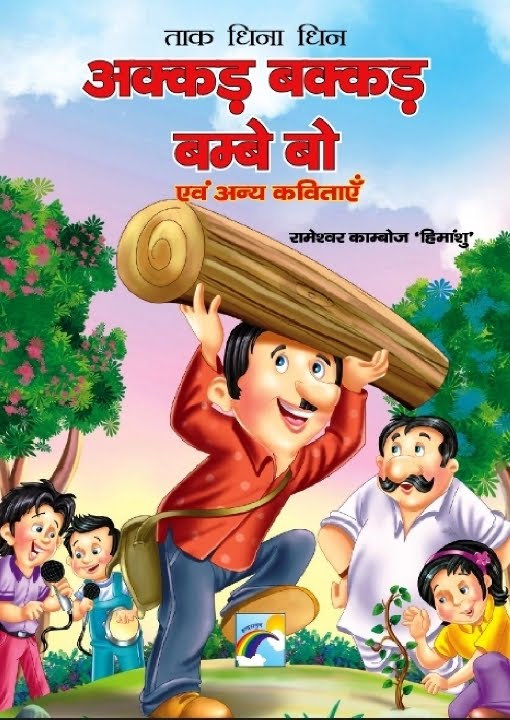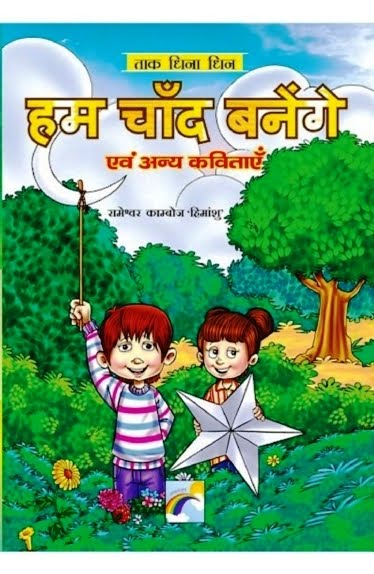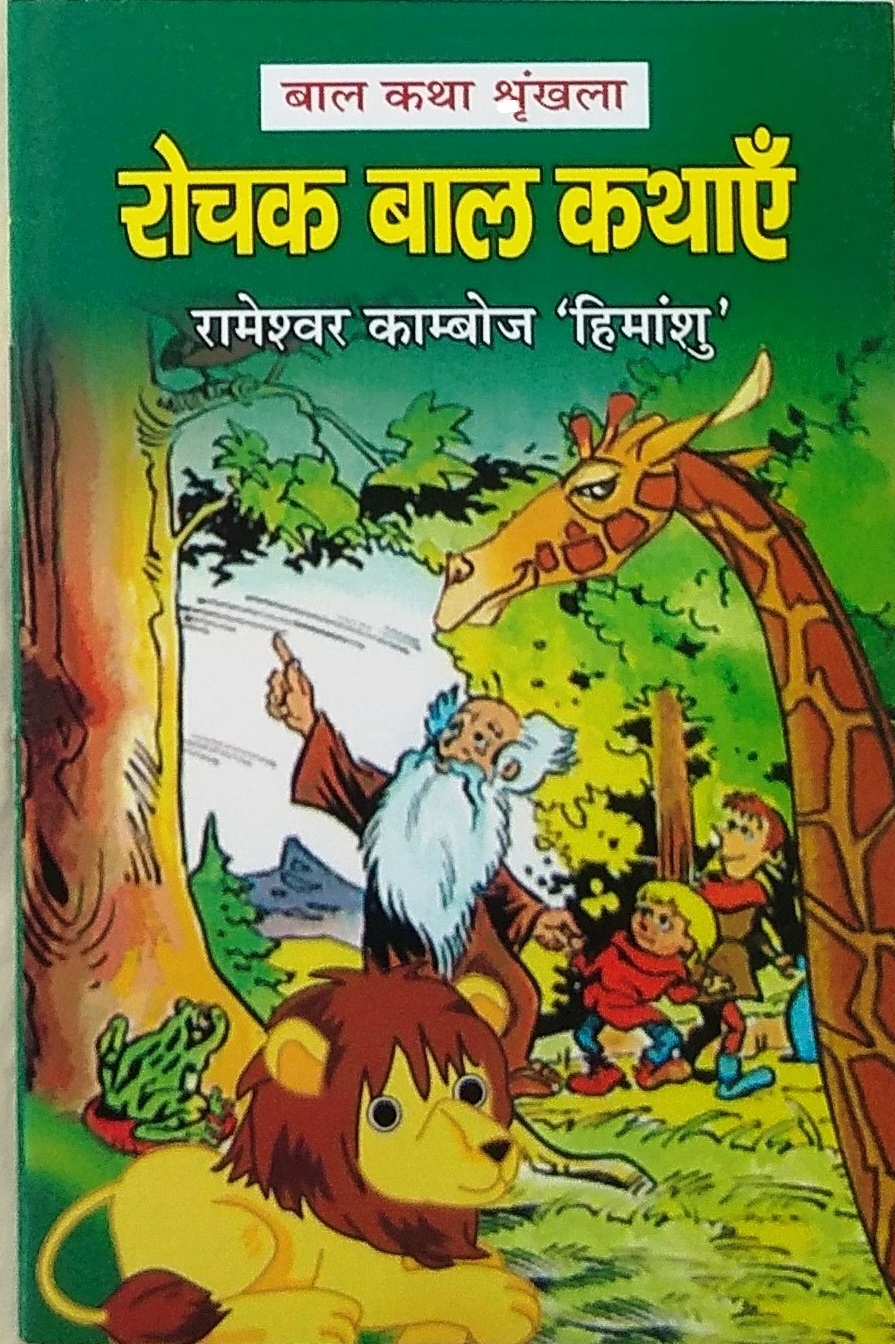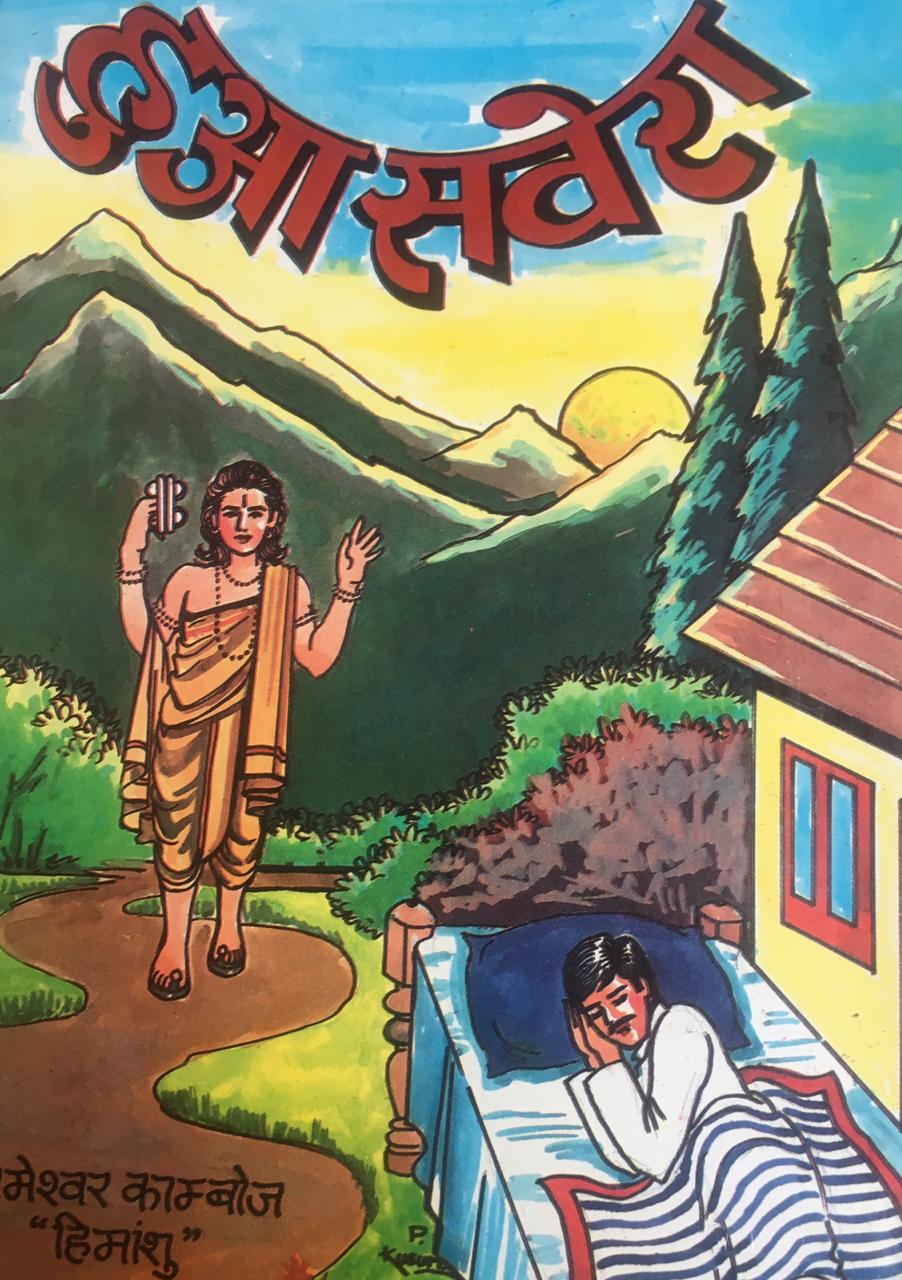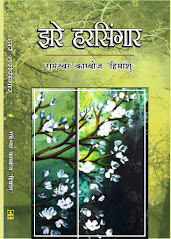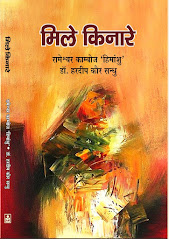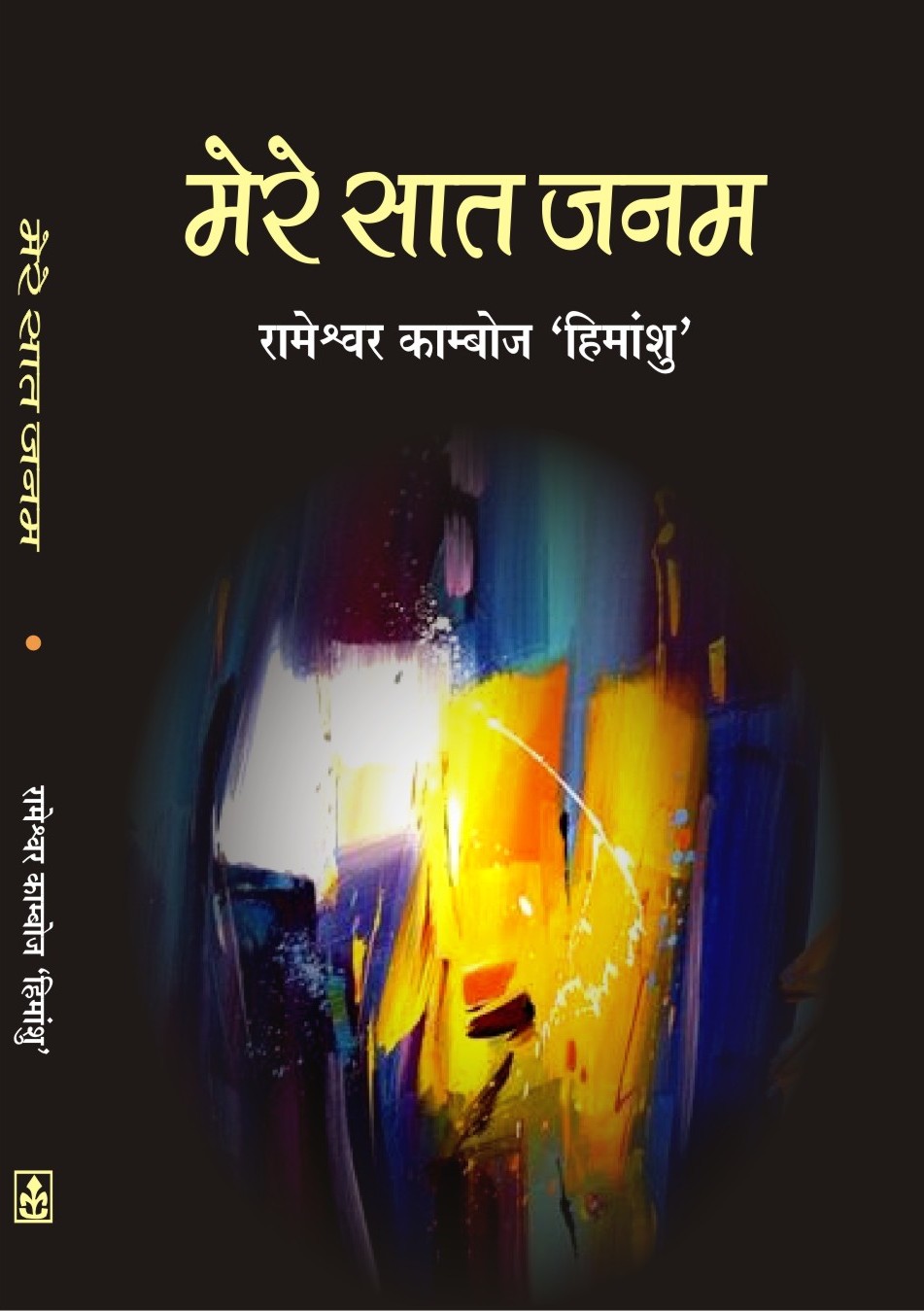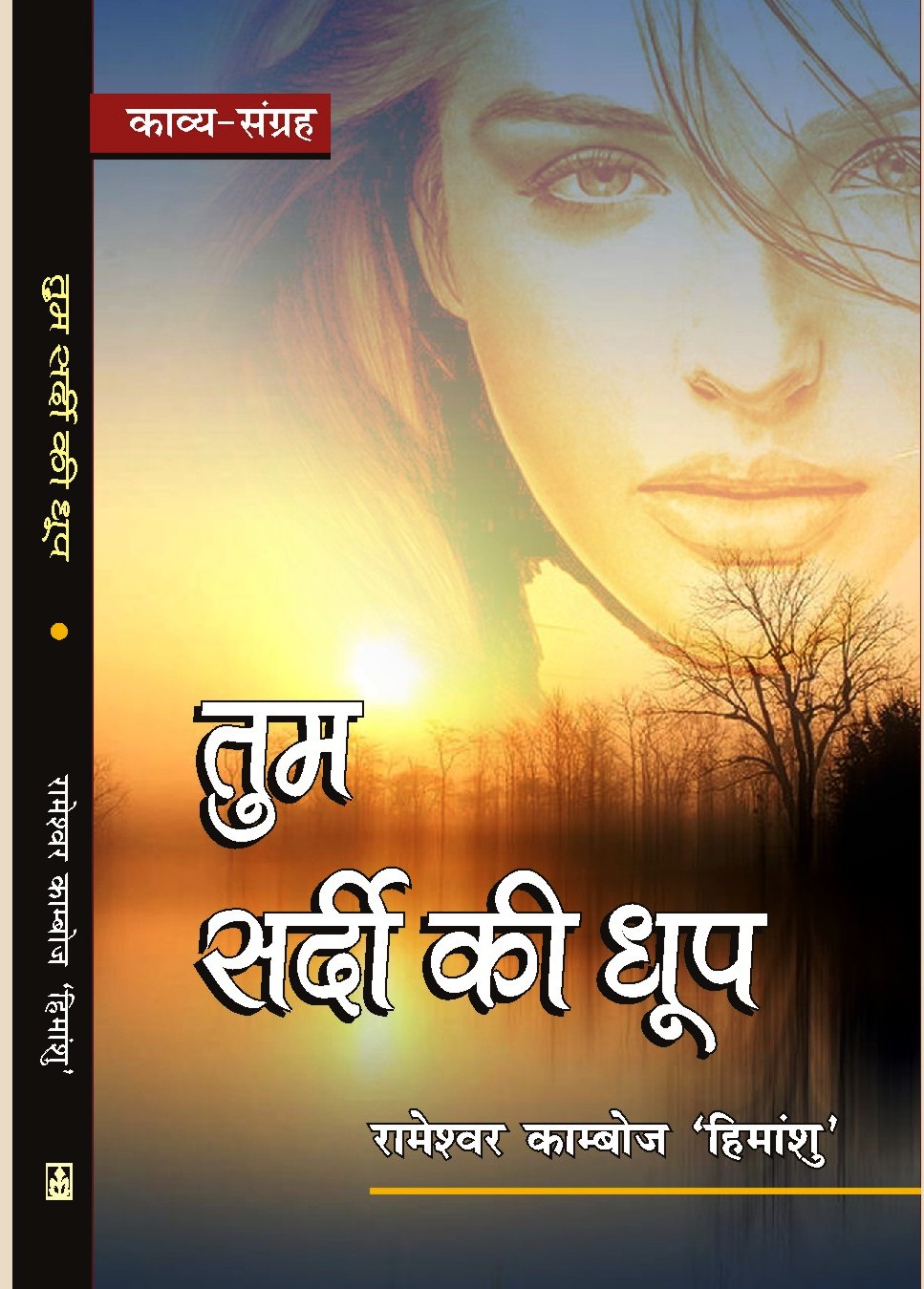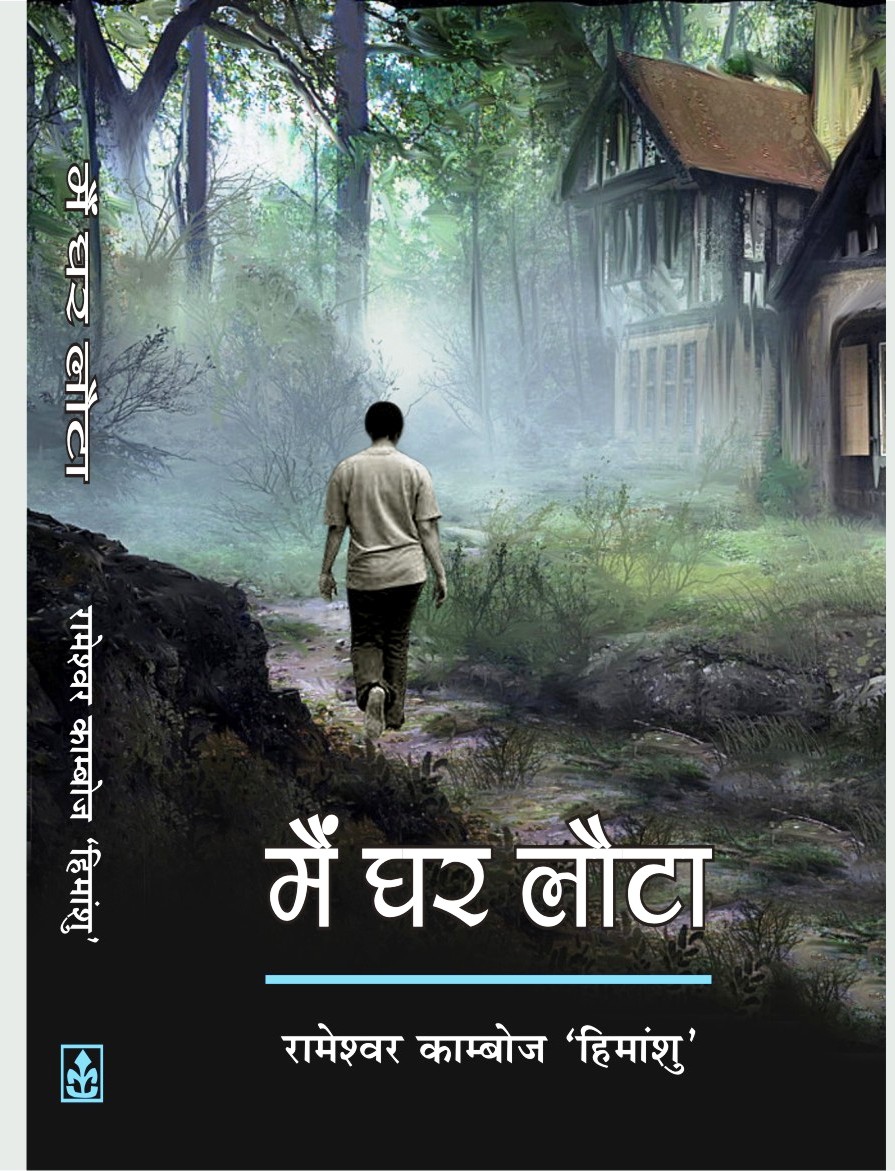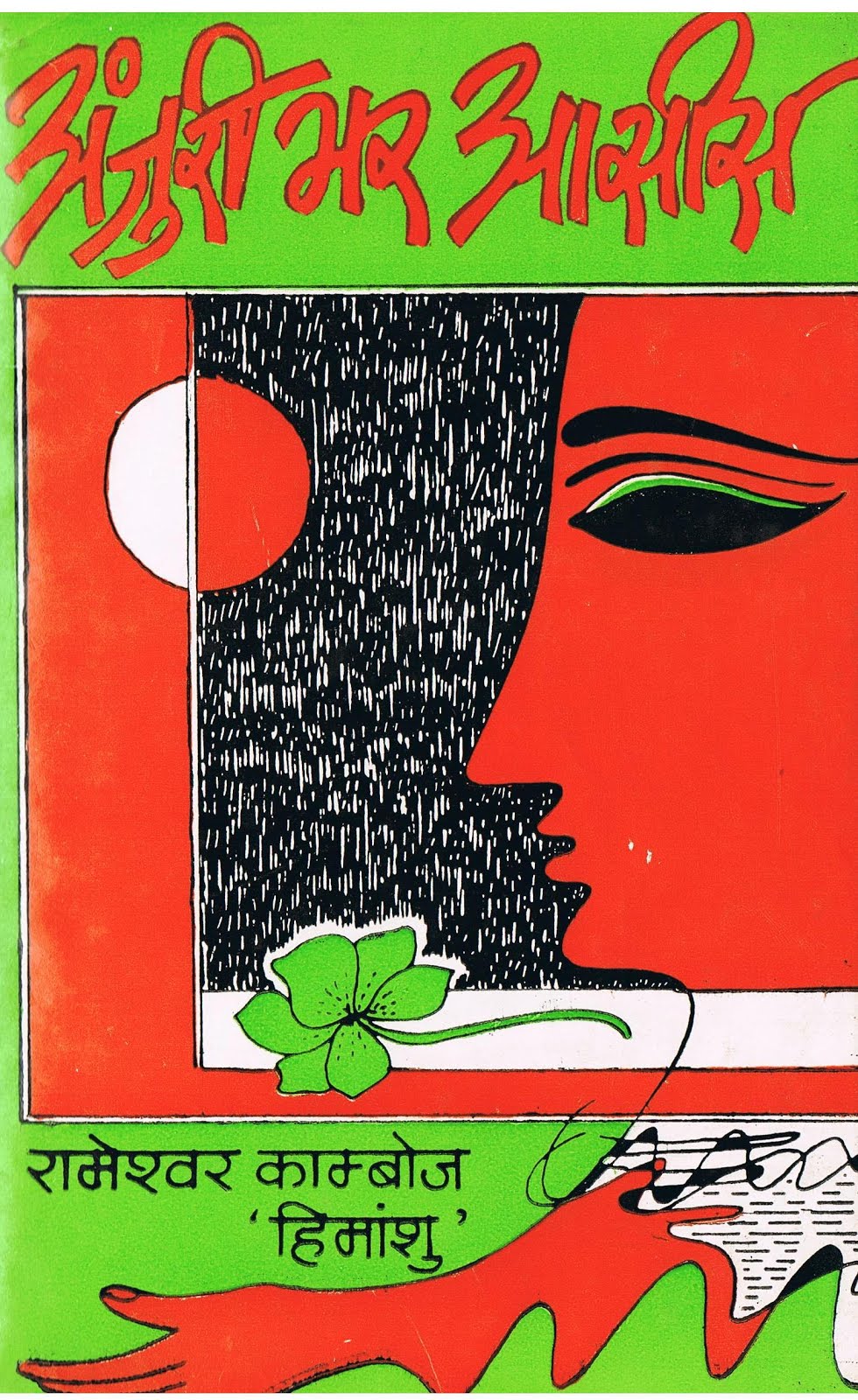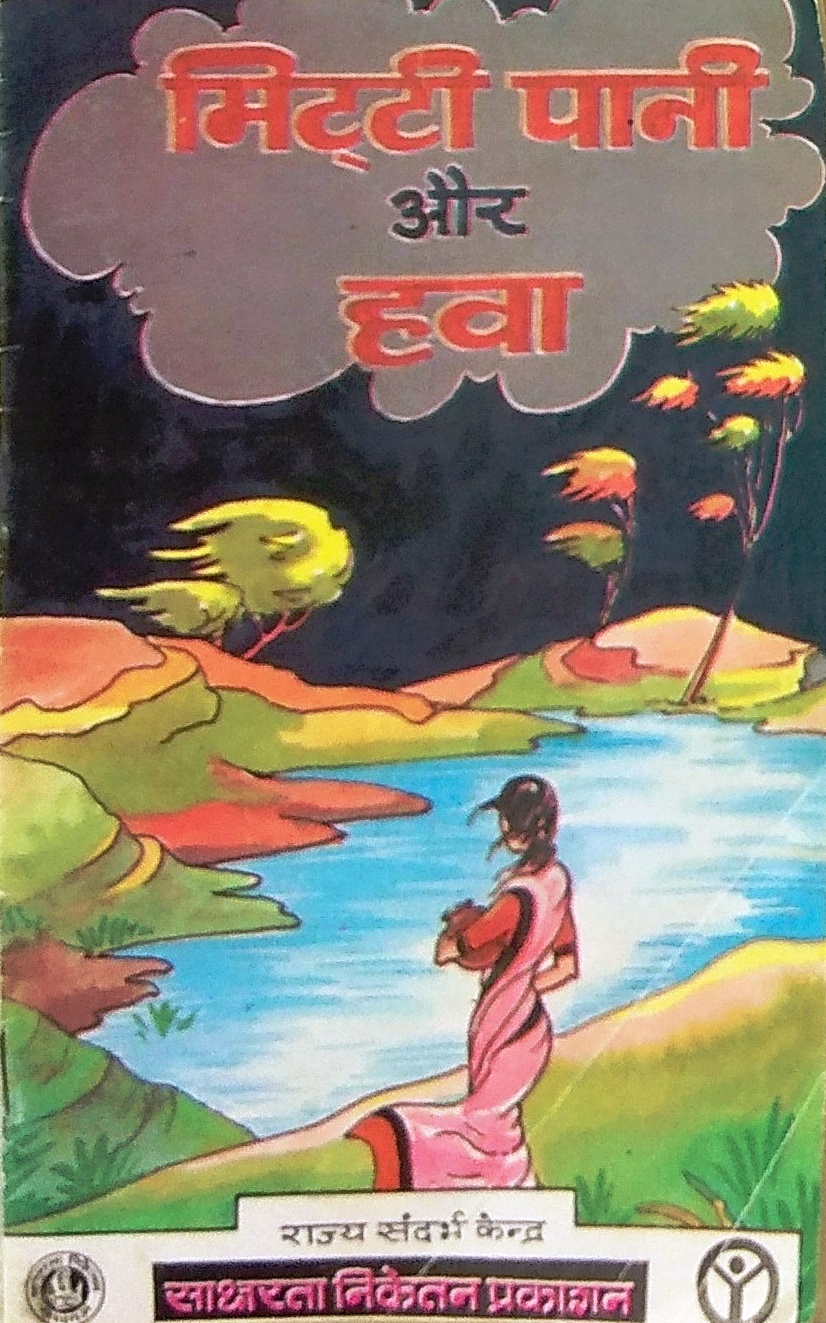रामेश्वर काम्बोज ‘हिमांशु’
सरूप जी का मकान पूछते–पूछते मैं परेशान हो चुका था। जब किसी से पता नहीं चला तो मैं ऑटो छोड़कर उस पॉश कॉलोनी में पैदल ही चल पड़ा। चिलचिलाती धूप में मेरा सिर चकराने लगा। कंठ प्यास के मारे सूख गया। ऐसे में कहीं से एक गिलास पानी मिल जाता।
सरूप जी ने कहा था–कभी इधर आओ तो ज़रूर मिलना। घूमते–भटकते नेम प्लेट पर दृष्टि पड़ी तो जान में जान आई। आँगन में मौलसिरी का छतनार पेड़ और उसके नीचे स्थापित सरस्वती की कमनीय मूर्ति। मन शीतल हो गया।
लोहे का भारी गेट दो बार खटखटाया। नारी–कंठ की समवेत खिलखिलाहट में खटखटाहट डूबकर रह गई। तीसरी बार गेट खटखटाने पर भीतर से ऊब भरी आवाज़ आई–‘‘कौन है भाई?’’
‘‘सरूप जी घर में हैं?’’ मैं गेट खोलकर आगे बढ़ा–‘‘मैं हूँ विजय प्रकाश। लखनऊ से आया हूँ।’’
‘‘विजय प्रकाश?’’ वे बाहर आकर अचकचाए। सामने के कमरे से कुछ नज़रें मुझे घूर रही थीं।
‘‘आपने पहचाना नहीं? पिछले साल अभिनंदन–समारोह में मिले थे हम लोग।’’
‘‘अरे हाँ, याद आया। आपने अभिनंदन–पत्र पढ़ा था।’’ वे माथे की सिलवटों पर हाथ फेरते हुए बोले–‘‘बहुत अच्छा पढ़ा था भाई आपने। सुबह ही बम्बई से लौटा हूँ। ‘कला भारती’ में कल मेरा सम्मान किया गया।’’
वे वहीं खड़े–खड़े आयोजन की गतिविधियाँ सुनाते रहे। मुझे थकान महसूस होने लगी। प्यास और तेज हो गई थी ;परन्तु पानी पीने की इच्छा जैसे मर चुकी थी।
‘‘कभी लखनऊ आना हो, मेरे यहाँ ज़रूर आइए......’’ मैंने सरूप जी को अपना कार्ड देते हुए आग्रह किया।
‘‘ज़रूर–ज़रूर...’’ उन्होंने कार्ड जेब में रखते हुए कहा।
‘‘अच्छा चलता हूँ जी।’’ मैंने अभिवादन की मुद्रा में हाथ जोड़े।
‘‘अच्छा!’’ कहकर उन्होंने जमुहाई ली।
मेरे मस्तिष्क में धुआँ–सा उठा। चलते समय मैंने एक दृष्टि सरस्वती की मूर्ति पर डाली। आँखों के आगे धुँधलापन छा गया। मूर्ति का केवल धड़ दिखाई दे रहा था। मैंने आखें मलीं पर बहुत प्रयास करने पर भी मूर्ति का सिर नहीं दिखाई दिया।
-0-